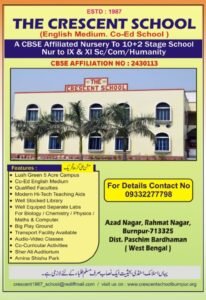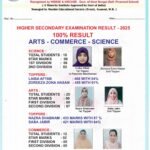“जोरा सांको की हवेली में,
जहाँ सुर और शब्दों की गूंज थी,
बंगाल की पावन माटी में,
एक रत्नभरा पुत्र की पूँज थी।
सन् अठारह सौ इकसठ का वह दिन,
वैशाख की रश्मियों में लहराता,
जब देवेंद्रनाथ की आँखों ने,
एक नव युग दृष्टि में पाया था।
रवीन्द्र! नाम में रवि की दीप्ति,
कांति में तेज, आँखों में राग,
बचपन से ही हठी, विचारी,
मन से विपुल, पर नितांत विराग।
विद्यालय की बंद सलाखें,
कभी उन्हें रास न आई,
शब्दों की दुनिया में वे खोए,
प्रकृति ने उनसे बातें बतलाई।
बड़ों के संग बहस करते,
कविताएँ सहज बहा देते,
बालक होते हुए भी भीतर,
युगों का ज्ञान छिपा देते।
घोड़े की पीठ हो या बगीचा,
या फिर बहता गंगा तट,
हर वस्तु में खोजें ईश्वर,
प्रकृति थी उनकी आत्मवृत्त।
माँ का साया जब छूट गया,
बालक मन हुआ अनाथ सा,
पर लेखनी बन गई सहारा,
दुख भी लगे प्रभु की बात सा।
भाई-बहनों में सबका चहेता,
संगीत जिसका प्राण-नाद,
संगीत सभा, ब्रह्म समाज,
सब उसकी गति के साथ।
उनके पिता – देवेंद्रनाथ,
ब्रह्म समाज के दीप समान,
बच्चे रबी को साथ ले जाते,
तीर्थों में, हिमालय की धाम।
वहाँ मिला प्रकृति का भान,
शब्दों में ढलते भाव महान,
पेड़, नदियाँ, पर्वत, धूप-छाँव,
बन गए कविता के वरदान।
संघर्षों की छाया में पला,
पर आत्मा से स्वतंत्र सदा,
कवि का जन्म नहीं होता है,
वह तो होता है स्वयं सृजा।
बालक रबी न था सामान्य,
वह था युगांतकारी स्वर,
जो शब्दों से रच दे जीवन,
और मौन से बोले अमर।”
*”भानुसिंह का उदय”
“जब बालक रबी किशोर बना,
और मन में भावों की लहर चली,
शब्दों ने ली कविता की वंशी,
और आत्मा सरगम में ढल चली।
नव तरुण रबी का हृदय,
भावों से भरा हुआ अंबर,
नयन देखते स्वप्न रंगीन,
और लेखनी करे अंतःस्तर।
तब जन्मा एक कवि गुप्त,
नाम रखा ‘भानुसिंह’ अद्भुत,
ब्रजभाषा में जब काव्य लिखा,
लगा जैसे राधा गा रही सुमधुर तुत।
भानुसिंह – वह था कवि का छद्म,
पर उसके शब्दों में नाद था सत्य,
कोई न जान सका यह रहस्य,
कि किशोर रबी ही यह चमत्कार रचत।
ब्रज की वंशी, वृंदा की छाया,
प्रेम की पीर, गोपियों की माया,
इन सबको रचा एक किशोर ने,
जैसे हो वाणी में रस की काया।
“बंधु मोरे, बरसाने जा रे”,
ऐसे गीत रचे जा रहे,
जनता समझे कोई अज्ञात संत,
पर रचयिता तो टैगोर खरे।
बिना विद्या के औपचारिक पट,
बिना विद्यालय की डिग्री सजी,
पर ज्ञान-गंगा हृदय में बहती,
जहाँ बुद्धि और भक्ति बसी।
उस युग में जब युवाओं को,
बस नौकरी की चिंता रही,
रबी ने शब्दों से राष्ट्र को,
एक नई चेतना दी सही।
उनका काव्य – श्रृंगार से प्रारंभ,
पर धीरे-धीरे बना राष्ट्रधर्म,
प्रेम, प्रकृति, आत्मा, करुणा,
और अंततः बन गया जनमर्म।
उनके गीतों में प्रकृति मुस्काई,
कभी कोयल की बोली बही,
कभी चाँदनी ने चिट्ठी लिखी,
कभी वर्षा ने कविता कही।
भाई-जगमोहन के साथ अंग्रेज़ी पढ़ी,
शेक्सपीयर, मिल्टन का रस लिया,
पर अंतर्मन का दीप जलाया,
भारत के स्वर में ही ज्ञान पिया।
जब अन्य किशोर खेल में मग्न थे,
रबी बना आत्मा का संवादक,
पन्नों पर लिखता आत्मगाथा,
बनता युगों का सृजनकारक।
भानुसिंह! तेरा नाम अमर है,
तू ही तो गुरुदेव की आरंभ गाथा है,
जहाँ से फूटी सृजन की धारा,
जो बहती है अब तक अथाह है।”
*”गीतों का गायक – राष्ट्र का नायक”
“जब जगा देश हृदय से सोकर,
और उठे स्वर भारत माता के,
तब गूँजा गगन में गीत अनुपम,
“जन गण मन अधिनायक जय हे”।
गुरुदेव की वह सधी लेखनी,
बन गई भारत की आत्मा,
हर स्वर, हर छंद, हर लय,
बोले भारत के वंदना का सपना।
“जन गण मन” न केवल गीत रहा,
वह तो युगों का आह्वान बना,
हर सैनिक की प्रेरणा वह,
हर जन-जन की पहचान बना।
गीतों में उन्होंने जीवन जिया,
कभी प्रकृति, कभी पीड़ा गाई,
कभी रबीन्द्र संगीत में उगता सूर्य,
कभी ‘गगन में थल में’ लहराई।
“एकला चलो रे” जब लिखा उन्होंने,
तब जैसे आत्मबल मुखर हुआ,
भीड़ की प्रतीक्षा मत कर तू,
तू ही दीप, तू ही स्वर हुआ।
महात्मा गांधी ने जिस गीत को,
अपना आत्मवाक्य बनाया,
वही गीत बना स्वतंत्रता का मंत्र,
जिसने भय को भी गाया।
“तू न चल सके तो मैं चलूँगा,
मैं न रुकूँगा, मैं न झुकूँगा”,
यह संकल्प गूँजा हर हृदय में,
जब टैगोर का स्वर बजा पूर्णा।
उनके गीतों में पीड़ा की पुलक थी,
कभी माता का क्रंदन था,
कभी कृषक की करुणा, कभी बालिका की मौन बिंधन था।
वह कवि न केवल प्रेम लिखे,
वह क्रांति की चिंगारी भी बने,
‘आमार सोनार बांग्ला’ जब उन्होंने रचा,
बांग्लादेश की आत्मा उसमें सजे।
राष्ट्रों की सीमाओं से परे,
उनके गीतों की ध्वनि चली,
मानवता, प्रेम, और करुणा की,
नई परिभाषा बनकर ढली।
गीत बनते गए संघर्ष के साथी,
जैसे बांसुरी युद्ध के वीरों की,
प्रकृति और मनुष्य का समन्वय,
उनके स्वर की यह हीरक थी।
उन्होंने नारी को नव रूप में देखा,
न वह अबला रही, न पराई,
रवीन्द्र के गीतों में वह शक्ति बनी,
जो बन जाए अग्निपरीक्षा की साई।
बालकों के लिए लिखा उन्होंने,
“চোখ খুলে দেখো, দেখে যাও রে”,
(अपनी आँखें खोलो, देखो !.)
मत कहो कि जग शुष्क है,
इसमें प्रेम की धार बहे।
उनकी लेखनी में जब संगीत गूँजा,
तब शांति निकेतन बना मंदिर,
जहाँ गीत बना शिक्षा, और शिक्षा बना प्रेम,
और हर शिष्य हुआ अंतर्मन का मंथन।
कभी माटी की गंध से गीत रचा,
कभी गांव की रज से रंग भरा,
कभी किसान के श्रम में काव्य लिखा,
कभी श्रमिक की हँसी में गीत गाया।
वह जनकवि थे, राष्ट्रकवि थे,
मानवता के परम व्रती थे,
गीतों में उन्होंने समाज को जोड़ा,
टूटते भारत को फिर से मोड़ा।”
*“विश्वकवि – नोबेल विजेता की गौरव गाथा”*
“जब शब्द बने प्रार्थना, और भाव हुए गगन सम,
तब गीतांजलि ने जन्म लिया,
कोमल छंदों में बसी आत्मा,
जिसमें स्वयं प्रभु ने स्वर दिया।
“Where the mind is without fear”
जब इंग्लैंड के हृदय में गूँजा,
तब यूरोप जागा, विश्व चकित,
और एक ऋषि का रूप संजीवनी में उतरा।
1913 की वह पुण्य घड़ी,
जब स्वीडन से संदेश आया,
“नोबेल पुरस्कार दिया जाता है,
भारत के उस महायोगी को,
जिसने कविता को प्रभु से मिलाया।”
गीतांजलि केवल कविता नहीं थी,
वह आत्मा की यात्रा बनी,
हर कविता में था ब्रह्म का प्रकाश,
हर शब्द में जीवन की धनी।
William Rothenstein ने देखा जब उन्हें,
तो बोला – “This man is a seer.”
And Yeats ने भूमिका लिख दी,
“These poems have the fire of prayer.”
“गीतांजलि” में जहां प्रकृति मुस्काई,
वहीं परमात्मा की छाया दिखी,
एक ऐसी भाषा जिसमें सभी धर्मों ने,
एक साथ शांति की ज्योति लिखी।
विश्व मंच पर भारत की वाणी,
पहली बार वह ऊँचाई पाई,
टैगोर ने न केवल पुरस्कार पाया,
भारत ने अपनी आत्मा दर्शाई।
यह नोबेल न केवल कवि को मिला,
यह तो भारत के ऋषि को था अर्पित,
जिसने विश्व को बताया –
“भारत की रचना में है अमर सृष्टि।”
वह विदेशों में गए, और बोल उठे –
“राष्ट्रवाद से ऊपर उठो मानवता में”,
उनका था स्पष्ट संदेश,
“मानव का बंधन केवल प्रेम में।”
जर्मनी से जापान, अमेरिका से फ्रांस,
हर राष्ट्र ने टैगोर9 को जाना,
भारत की मिट्टी से जन्मे ऋषि को,
विश्व ने अपना गुरु माना।
“Internationalism” बना उनका मन्त्र,
“Viswa Bharati” बना उनका यज्ञस्थल,
जहाँ भारत और विश्व जुड़े,
ज्ञान, कला, और मानवतावाद में अटल।
पर नोबेल के बाद भी वह नम्र रहे,
बोले – “यह प्रभु की कृपा है”,
“मैं तो केवल एक डाकिया हूँ,
जो ब्रह्म का संदेश लिए चला है।”
*“शांति का शिल्पकार – शिक्षा, विश्वभारती और मानवतावाद”*
“जब नोबेल की गूंज मिटी,
और लौटी आत्मा अपनी भूमि,
तब गुरुदेव ने देखा स्वप्न,
जो था न राजमहल, न कृति कोई जमीं।
बल्कि एक आश्रम, वृक्षों की छाँव में,
जहाँ खुले आकाश की गोद में
बच्चा सीखे प्रकृति से,
न दीवारों में कैद, न घंटियों की बाधा में।
शांति निकेतन – उन्होंने नाम दिया,
जहाँ ज्ञान हो जीवन का अंग,
ना सिर्फ पाठ्यक्रम, ना सिर्फ अंक,
बल्कि आत्मा की यात्रा का संग।
“Education is not the filling of a pail,
but the lighting of a fire” –
उनका ये दर्शन बना दीप,
जो जलाए हर हृदय में विचार।
गुरुदेव बोले – “Nature is the first teacher,”
पेड़ की छाँव, नदियों की धुन,
सूरज की रोशनी, चिड़ियों की चहचहाहट,
यही है जीवन का प्रथम पाठशाला-गुन।
उन्होंने विद्यालय को बनाया आश्रम,
जहाँ शिक्षक न राजा, न व्यापारी,
बल्कि साथी थे ज्ञान की यात्रा में,
और विद्यार्थी न गुलाम, न अधिकारी।
विश्वभारती – फिर हुआ जन्म एक स्वप्न का,
“जहाँ विश्व धरती से हो एक,”
“Where the world makes a home in a nest of peace,”
जहाँ न जात-पात, न धर्म का क्लेश।
He wrote: “India is not for Indians alone.
She is for the world,”
And so in the soil of Santiniketan,
He sowed the seeds for a better world.
कहीं जापानी छात्र बांसुरी बजाता,
तो कहीं फ्रांसीसी विद्या में खो जाता,
विश्व से छात्र आए वहाँ,
ज्ञान और आत्मा का संगम वहाँ।
शांतिनिकेतन बना प्रतीक,
एक ऐसे भारत का जो खुले विचारों वाला,
जहाँ वेद, उपनिषद और विज्ञान,
संग रहते एक आत्मीय हाला।
गुरुदेव ने कहा –
“True education is that which liberates,”
“जो बनाता है इंसान को सहृदय,
जो जोड़ता है मानवता के द्वार।”
हिंदी, बांग्ला, अंग्रेज़ी, जापानी,
हर भाषा में एक ही संदेश,
“हम सब एक हैं, यह पृथ्वी हम सबकी है,”
यही था विश्वभारती का विशेष।”
*“क्रांति और करुणा – स्वतंत्रता संग्राम में टैगोर की भूमिका”*
“जब भारत में चिंगारी सीली थी,
ब्रिटिश तिमिर ने ज़िंदगी को घेर लिया,
तब एक आवाज़ उठी, लेकिन न वह केवल गुस्सा थी,
वह थी प्रेम की पुकार, हर दिल में जो उबली थी।
रवीन्द्रनाथ टैगोर, जो थे शांति के पुजारी,
उन्होंने देखा सोलह वर्षों से दबा एक विचार,
“भारत को चाहिए स्वाधीनता, न भय, न विवशता,”
अंग्रेज़ों के शासन में, हो रहे हर सुख का नाश।
स्वतंत्रता का स्वप्न उनके दिल में पलता,
नफ़रत की जगह, प्रेम का बीज बोता,
“एक सभ्यता है जो पूरी दुनिया को जोड़ती,”
यह संदेश हर स्वर में, हर कविता में खोता।
जैसे ही आंदोलनों की लहर बढ़ी,
और ‘स्वदेशी आंदोलन’ ने दस्तक दी,
रवीन्द्रनाथ का कलम हुआ धारदार,
उनके गीत, कविताएँ बन गईं आंधी की मार।
लेकिन वह थे न केवल क्रांतिकारी विचारक,
बल्कि करुणा के भी सच्चे आस्थावान,
“गांधीजी,” उन्होंने कहा, “है सत्य का रक्षक,
वह मार्गदर्शक जो हमें दे सकता है क्रांति का जीवनदान।”
उनकी कविताएँ, उनके गीत,
जैसे सूरज की किरण बिखरे रात्रि की गहरी चुप में,
भारत की आत्मा को जगाने वाली थीं,
कभी न थमने वाली, कभी न रुकने वाली थीं।
लेकिन एक दिन, जब ब्रिटिश सम्राट ने उन्हें नाइटहुड का सम्मान दिया,
रवीन्द्रनाथ ने कहा – “न, यह मेरे भारत की स्वाभिमान का अपमान है,”
उन्होंने लौटाया वह पद, जो था सम्राट से स्वीकार,
क्योंकि उनका आत्मसम्मान था उनके देश के साथ प्यार।
उन्होंने ना कभी सत्ता की आकांक्षा की,
ना कभी अंधी तिजोरी की दौलत की,
उनकी जड़ें थीं धरती में, हृदय में भारत था,
उनके मन में केवल एक सपना था – स्वाधीन भारत का मार्गदर्शन।
“स्वाधीनता केवल धरती पर नहीं,
यह है आत्मा की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति,”
रवीन्द्रनाथ ने यह कविता लिखी,
जो थी सत्य के उस महान संदेश की पुष्टि।
गांधीजी और रवीन्द्रनाथ, दो दीपक एक ही आकाश में,
एक ने सत्य को जाना, दूसरे ने अहिंसा को,
दोनों का संगम बना, वह भारतीय क्रांति का अद्वितीय भाग,
जो हो गया मुक्त, एक नई राह की ओर रौशन होने वाला।
रवीन्द्रनाथ ने समझा,
“हर स्वतंत्रता का अर्थ है मानवता का सम्मान,”
हर नागरिक, हर बच्चा, हर स्त्री, हर युवा,
अपने अधिकारों से संपन्न हो, यह है उनका मानवता का संकल्प।
रवीन्द्रनाथ टैगोर की यह काव्य-यात्रा,
क्रांति और करुणा का मिश्रण था,
उन्होंने जिया न केवल अपनी कविता में,
बल्कि उन्होंने स्वाधीनता के लिए अपने अस्तित्व को समर्पित किया था।”
*“कवि: सुशील कुमार सुमन”*
अध्यक्ष, आईओए
सेल आईएसपी बर्नपुर